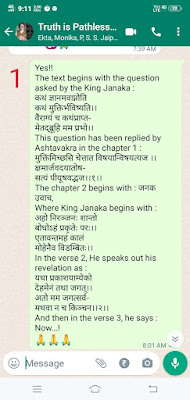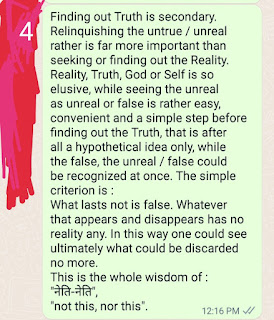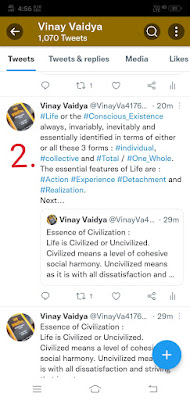Veda, Upanishad and Purana
----------------------©---------------------
वेद, उपनिषद् और पुराण
।।प्रह्लादकृत नृसिंह स्तोत्रम्।।
--
प्रह्लाद उवाच :
(१ से २२ तक.... और इसी क्रम में आगे ...)
एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्व-
माद्ययन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च।।
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं
नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः।।२३।।
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो
माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था।।
यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च
तद्वै तदेव वसुकालवदिष्टतर्वोः।।२४।।
न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये
शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः।।
योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्र-
स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे।।२५।।
तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या
सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्।।
अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधे-
र्नाभेरभूत्स्वकणिकावटवन्हाब्जम्।।२६।।
तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमान-
स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य।।
नाविन्दब्दशतमप्सु निमज्जमानो
जातेऽङ्कुरे कथमु होपलभेत बीजम्।।२७।।
स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः।।
त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं
भूतेन्द्रियाशमये विततं ददर्श।।२८।।
एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरःकरोरु-
नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्।।
मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं
दृष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः।।२९।।
(इति यथा प्रह्लादकृत नृसिंहस्तोत्रे वर्णितम्)
स एव ब्रह्मा,
देवानां प्रथमः सम्बभूव,
इति मुण्डकोपनिषदि यथा हि --
प्रथम मुण्डक, प्रथम खण्ड --
ॐ ब्रह्मा हि देवानां प्रथमः सम्बभूव
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।।
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा-
मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह।।१।।
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा-
थर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्।।
स भारद्वाजाय सत्यवहाय
प्राह भारद्वजोऽङ्गिरसे परावराम्।।२।।
शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ।।
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति।।३।।
तस्मै स होवाच। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैवापरा च।।४।।
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति।
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।।५।।
ब्रह्मविद्या हि ब्रह्माणी अथ सरस्वती।।
अथ गङ्गा च यमुना द्वे हिमवान्कन्ये।।
गङ्गा सुरसरिः।।
यमुना च सूर्यजाता यमधर्मिणी।।
अपि च सरयू इति अयोध्यातटवाहिनी।।
तमसा इति वैतरणी।।
अङ्गिरा गिरा च वाक् वाचा वाणी वैखरी ध्वनिरूपा सरस्वती।।
अङ्गिरया आङ्लभाषा व्युत्पन्ना।।
गिरया च ग्रीकभाषा ग्रीञ्च ग्रीस् इति।।
सरस्वती विशुद्धा निराकार निर्गुणा विलुप्ति आध्यात्मिका च।।
गङ्गा सतोरूपा काशीतलवाहिनी देवसरिता आधिदैविकी ।।
यमुना यमस्य सहजाता रजोगुणी यमधर्मिणी आधिभौतिका लौकिकी च।।
यमस्य यमुना यामिनी, तमस्य तमसा।।
अथ *इल आख्यानम् --
यथा हि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्ताशीतितमे सर्गे --
तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः।।
प्रत्युवाच महातेजाः प्रहसन् राघवो वचः।।१।।
एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण।।
वृत्रघातमशेषेण वाजिमेधफलं तथा।।२।।
श्रूयते हि पुरा सौम्य कर्दमस्य प्रजापतेः।।
पुत्रो बाह्लीश्वरः श्रीमान् *इलो नाम सुधार्मिकः।।३।।
स राजा पृथिवीं सर्वां वशे कृत्वा महायशाः।।
राज्यं चैव नरव्याघ्र पुत्रवत् पर्यपालयत्।।४।।
सुरैश्च परमोदारैर्दैतेयश्च महाधनैः।।
नाग-राक्षस-गन्धर्वैर्यक्षैश्च सुमहात्मभिः।।५।।
पूज्यते नित्यशः सौम्य भयार्तै रघुनन्दन।।
अबिभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः।।६।।
स राजा तादृशोऽप्यासीद् धर्मे वीर्ये च निष्ठितः।।
बुद्ध्या च परमोदारो *बाह्लीकेशो महायशाः।।७।।
स प्रचक्रे महाबाहुर्मृगयां रुचिर घने।।
चैत्रे मनोरमे मासे सभृत्यबलवाहनः।।८।।
(चैत्रं तु प्रथमं मासं संवत्सरे यथा प्राप्तम्।
संवत्सरं तथैव तत् काले नित्यं प्रवर्तते।।)
शिवक्षेत्र, *बाह्लीक, *इल, इला और इलावर्त
--
प्रजघ्ने स नृपोऽरण्ये मृगाञ्शतसहस्रशः।।
हत्वैव तृप्तिर्नाभूच्च राज्ञस्तस्य महात्मनः।।९।।
नानामृगाणामयुतं वध्यमानं महात्मना।।
यत्र जातो महासेनस्तं देशमुपचक्रमे।।१०।।
तस्मिन् प्रदेशे देवेशः शैलराजसुतां हरः।।
रमयामास दुर्धर्षः सर्वैरनुचरैः सह।।११।।
कृत्वास्त्रीरूपमात्मानमुमेशो गोपतिध्वजः।।
देव्याः प्रियचिकीर्षुः संस्तस्मिन् पर्वतनिर्झरे।।१२।।
यत्र यत्र वनोद्देशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः।।
वृक्षाः पुरुषनामानस्ते सर्वे स्त्रीजना भवन्।।१३।।
यच्च किञ्चन तत् सर्वं नारीसंज्ञं भभूत ह।।
एतस्मिन्नन्तरे राजा स *इलः कर्दमात्मजः।।१४।।
निघ्नन् मृगसहस्राणि तं देशमुपचक्रमे।
स दृष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सव्याल मृगपक्षिणम्।।१५।।
आत्मानं स्त्रीकृतं चैव सानुगं रघुनन्दन।।
तस्य दुःखं महच्चासीद् दृष्ट्वाऽऽत्मानं तथागतम्।।१६।।
उमापतेश्च तत् कर्म ज्ञात्वा त्रासमुपागमत्।।
ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम्।।१७।।
जगाम शरणं राजा सभृत्यबलवाहनः।।
ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः।।१८।।
प्रजापतिसुतं वाक्यमुवाच वरदः स्वयं।।
उत्तिष्ठैत्तिष्ठ राजर्षे कार्दमेय महाबल।।१९।।
पुरुषत्वमृते सौम्य वरं वरय सुव्रत।।
ततः स राजा शोकार्थः प्रत्याख्यातो महात्मना।।२०।।
स्त्रीभूतोऽसौ न जग्राह वरमन्यं सुरोत्तमात्।।
ततः शोकेन महता शैलराजसुतां नृपः।।२१।।
प्रणिपत्य उमां देवीं सर्वेणैवान्तरात्मना।।
ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी।।२२।।
अमोघदर्शने देवि भज सौम्येन चक्षुषा।।
हृद्गतं तस्य राजर्षेर्विज्ञाय हरसंनिधौ।।२३।।
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता।।
अर्धस्य देवो वरदो वरार्धस्य तव ह्यहम्।।२४।।
तस्मादर्धं गृहाण त्वं स्त्रीपुंसोर्यावदिच्छसि।।
ततद्भुतं श्रुत्वा देव्या वरमनुत्तमम्।।२५।।
सम्प्रष्टमना भूत्वा राजा वाक्यमथाब्रवीत्।।
यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा भुवि।।२६।।
मासं स्त्रीमुपासित्वा मासं स्यां पुरुषः पुनः।।
ईप्सीतं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना।।२७।।
प्रत्युवाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति।।
राजन् पुरुषभूतस्त्वं स्त्रीभावं न स्मरिष्यसि।।२८।।
स्त्रीभूतसश्च परं मासं न स्मरिष्यसि पौरुषम्।।
एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वाथ कार्दमिः।।
त्रैलोक्यसुन्दरी नारी मासमेकमिलाभवत्।।२९।।
कौन है यह राजा प्रजापति कर्दम के कुल में उत्पन्न हुआ था और जिसका सम्पर्क बाद में इल तथा इला के रूप में महात्मा बुध से हुआ। इला के रूप में स्त्री रूप में होने पर बुध से उनका पुत्र चन्द्रमा हुआ। इला और इल से ही ऐल (जैन) धर्म का कोई संबंध है। इससे ही ऐलाचार्य शब्द बना। अरबी भाषा में ऐलची भी इस से ही व्युत्पन्न या अपभ्रंश है जिसका अर्थ 'दूत' होता है। संस्कृत भाषा में 'अल्' प्रत्यय पूर्णता का द्योतक है, जैसा कि -- अलंकरण, अलंकृत, अलंकार आदि में दृष्टव्य है। यह उपसर्ग (prefix) एवं समास (suffix) दोनों ही तरह से संस्कृत के ही साथ साथ अरबी, लैटिन, और अंग्रेजी भाषाओं में भी इसी अर्थ का द्योतक है - जैसे all, et al, में। आलम अर्थात् संसार तो प्रसिद्ध है ही।
ज्योतिषीय दृष्टि से भी बुध जो नपुंसक ग्रह माना जाता है इसी आधार पर एक मास तक स्त्री और अगले एक मास तक पुरुष की भूमिका में होता है। चन्द्रमा का एक मास लगभग 27 से 28 दिनों तक की अवधि का होता है, जबकि सूर्य का लगभग 30 से 31 दिनों तक की अवधि का।
वाल्मीकि रामायण में ज्योतिषीय तथ्यों का जैसा उल्लेख पाया जाता है उससे यही सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ के सभी पात्रों की भूमिका अधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक स्तरों पर एक साथ सत्य है। इस ग्रन्थ से वेदों, उपनिषदों और पुराणों के मध्य सुसंगति खोजने और स्थापित करने के लिए सहायता भी मिलती है।
***
इति अलम्।।
Cognates :
James, Thames, Angel, Anglo, Greece, Greek,